
क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी प्राचीन समय से ही भारत में ऊसर (बंजर) या रेह के नाम से जानी जाती है| आज से लगभग 157 वर्ष पहले, नहर द्वारा सिंचाई शुरू होने के उपरान्त से इस समस्या की गम्भीरता को महसूस किया गया, पहली बार एक किसान ने सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया| तब से आज तक क्षारीय एवं लवणीय समस्या का आकार प्रति वर्ष बढ़ा है|
क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी की पहचान, क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी के अनुसार पोषक तत्वों और उर्वरकों , क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी में पानी का उपयोग की जानकारी इत्यादि को ध्यान में रखकर किसान बन्धु क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी से भी फसल की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते है, इस लेख द्वारा क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी में पोषक तत्वों का प्रबंधन उल्लेख किया गया है, जिनका उपयोग कर के क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी में भी अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है|
यह भी पढ़ें- क्षारीय एवं लवणीय जल का खेती में सुरक्षित उपयोग कैसे करें
क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी की पहचान और सुधार
क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी प्रायः शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पायी जाती हैं, इनके बनने की मुख्य भूमिका में निम्नलिखित कारक अहम् होते हैं, जैसे-
1. शुष्क जलवायु,
2. बहुत समय तक अधिक लवणीय जल द्वारा सिंचाई करना,
3. जल निकास की कमी,
4. उच्च भौम जल स्तर,
5. प्रोफाइल में कड़ी परत,
6. मूल पदार्थों की प्रकृति,
7. क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग,
8. समुद्री जल में अनेक प्रकार के विलेय लवण होने के कारण, इस जल का मिट्टी के ऊपर से बहने पर भी मिट्टी लवणग्रस्त बन जाती है,
9. हल के तालू की रगड़ाई से पतली कड़ी पर्त बनना|
यह भी पढ़ें- फसलों या पौधों में जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु रासायनिक एवं कार्बनिक खादें
लेकिन इन कारकों के अलावा कुछ अध्ययनों से पता चलता है, कि सिंचित क्षेत्रों में जलमग्नता और लवणीयता की समस्या के संभावित कारण इस तरह हैं, जैसे-
1. नहरी जलतन्त्र से पानी का रिसाव,
2. फसलों में असंतुलित सिंचाई,
3. सतही निकास में रूकावट,
4. स्थानीय तलरूप एवं जलवायु।
लवण ग्रस्त मिट्टियों में आमतौर पर दो तरह की मृदायें होती हैं, जैसे-
1. लवणीय मिट्टी,
2. क्षारीय मिट्टी|
लवणीय मिट्टी की पहचान क्या है?
लवणीय मिट्टी का तात्पर्य है, कि मिट्टी में घुलनशील लवणों की अधिक मात्रा के कारण बीज का अंकुरण और विकास पर बुरा प्रभाव होता है| इन मिट्टी के संतृप्त निष्कर्ष की वैद्युत चालकता 4 डेसी सीमन प्रति मीटर से अधिक (25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर) और मिट्टी पी एच मान 8.2 से कम होता है| ऐसी मिट्टी में विनियम योग्य सोडियम 15 प्रतिशत से कम होता है| लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्सियम, मैग्निशियम और उनके क्लोराइड तथा सल्फेट अधिक मात्रा में पाये जाते हैं|
पहचान- खेतों में लवणीय मिट्टी की पहचान फसलों की कुछ विशेष क्षेत्र (चकत्तियां) में कम बढ़वार होती है| भूमि की सतह पर सफेद रंग की पपड़ी का जमाव दिखता है, जो मिट्टी को पहचानने में सहायक होती है| कभी-कभी इनकी पहचान लवण क्षति, जैसे पत्तियों के अग्र सिरों का झुलसाना और पत्तियों की हरिमाहीनता हल्का पीला रंग के द्वारा भी की जाती है| ऐसी मृदाओं द्वारा वातावरण से नमी सोखने के कारण गीली-गीली सी लगती है| जो अधिक मात्रा में लवणों के कारण नमी को वातावरण से सोखा जाता है| जबकि ऐसी मिट्टी में परासरण दाब के कारण पौधों के लिए प्राप्य जल की कमी होती है|
यह भी पढ़ें- गेहूं की उत्तम पैदावार के लिए मैंगनीज का प्रबंधन
क्षारीय मिट्टी की पहचान क्या है?
क्षारीय मिट्टी में कैल्शियम, मैग्निशियम और पोटेशियम आदि विनिमय धनायनों के साथ सोडियम भी मृदा कोलाइडी कणों पर अधिशोषित होता है, जैसे-जैसे मिट्टी में सोडियम का सान्द्रेण बढ़ता जाता है| वह दूसरे धनायनों को वहाँ से विस्थापित कर देता है| इसीलिए क्षारीय मिट्टी के संतृप्त निष्कर्ष का पी एच मान 8.2 से अधिक, विद्युत चालकता 4 डेसी सीमन प्रति मीटर से कम (25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर) और विनिमय योग्य सोडियम 15 प्रतिशत से अधिक होता है|
पहचान- क्षारीय मिट्टी की पहचान लवणीय मिट्टी की अपेक्षा कठिन है| वर्षा ऋतु में पानी काफी समय तक भरा रहता है| क्षारीय मिट्टी गीली होने पर चिकनी हो जाती है| इसमें उपरी सतह पर भरा पानी गंदला रहता है| क्षारीय मिट्टी में सूखने पर काफी बड़ी दरार आ जाती है| कभी-कभी कार्बनिक पदार्थ जल में घुलकर मिट्टी की उपरी सतह को काली कर देती है| कभी-कभी कुछ पौधों की पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है और पौधे झुलसे हुए दिखाई देते हैं| क्षारीय मिट्टी में पौधों की वृद्धि बहुत कम होती है या अंकुरण होता ही नहीं है|
यह भी पढ़ें- धान व गेहूं फसल चक्र में जड़-गांठ सूत्रकृमि रोग प्रबंधन
क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी में पोषक तत्वों के कार्य
क्षारीय मिट्टी में अधिकांशत- नाइट्रोजन, कैल्शियम, जिंक और कभी-कभी मैंगनीज पोषक तत्वों की कमी होती है|
नाइट्रोजन के कार्य- नाइट्रोजन पोषक तत्व फसलों के लिए मुख्य पोषक तत्व माना जाता है| पौधों में नाइट्रोजन नियन्त्रक का काम करता है| इससे फास्फोरस और पोटेशियम का विनियम भी संतुलित रहता है| साथ ही साथ यह पौधों में फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम को शोषित करने की क्षमता को बढ़ाता है| नाइट्रोजन क्लोरोफिल के संश्लेषण में भाग लेता है और सभी प्रोटीनों का आवश्यक अवयव होता है|
कैल्शियम के कार्य- कैल्शियम पौधों के जड़ों के शिरों के विभज्योतकों में सामान्य कोशिका विभाजन को बढ़ाता है| यह बीज निर्माण को उत्साहित करता है, कैल्शियम पौधों की मेटाबोलिज्म में स्वतन्त्र हुए कार्बनिक अम्लों को उदासीन करता है| इस प्रकार यह एक अविष्कारी कारक का कार्य करता है| शर्करा के प्रभाव में मदद और पौधों में पानी की पूर्ति में सहायक होता है|
जिंक के कार्य- जिंक पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले पदार्थ ऑक्सीजन के सान्द्रंण को नियमित करता है| यह कार्बोहाइड्रेटस के रूपान्तरण में आवश्यक है एवं क्लोरोफिल निर्माण के समय उत्प्रेरक का कार्य करता है| पौधों की जटिल प्रक्रियाओं तथा नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की उपयोग में सहायक होता है|
मैंगनीज के कार्य- मिट्टी से पौधों द्वारा जल के अवशोषण को बढ़ाता है| मैंगनीज क्लोरोप्लास्ट का एक प्रमुख अवयव है तथा उन क्रियाओं में भाग लेता है, जिनमें ऑक्सीजन मिलती है| प्रकाश संश्लेषण में सुधार के साथ-साथ नाइट्रोजन उपापचय में सुधार करता है|
इन पोषक तत्वों की कार्य प्रणाली से यह पता चलता है कि प्रत्येक पोषक तत्व किसी न किसी रूप में अपना सहयोग पौधों के जीवन चक्र में देते हैं, यदि इस तरह पोषक तत्वों में से किसी एक की मिट्टी में कमी होने पर वह तत्व अपनी कमी के लक्षण प्रदर्शित करता है| हमेशा आवश्यक पोषक तत्व की कमी को केवल उसी तत्व को मिट्टी में प्रदान करके दूर किया जा सकता है यानि की एक तत्व को दूसरे तत्व से पूरा नहीं किया जा सकता है|
यह भी पढ़ें- स्वस्थ नर्सरी द्वारा बासमती धान की पैदावार बढ़ाये
क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के पौधों पर लक्षण
नाइट्रोजन की कमी के पौधों पर लक्षण-
1. पौधों की वृद्धि में रुकावट आती है|
2. पौधों की पुरानी पत्तियों का रंग पीला हो जाता है|
3. गेहूं तथा अन्य फसलें जिनमें कल्ले (टिलर) निर्माण होता है, नाइट्रोजन की कमी से कल्ले कम बनते हैं|
4. पत्तियों का रंग सफेद हो जाता है तथा कभी-कभी पत्तियां जल भी जाती हैं|
5. हरी पत्तियों के बीच-बीच में सफेद धब्बे पड़ जाते हैं|
6. दाने वाली फसलों में सबसे पहले पौधों की निचली पत्तियाँ सूखना आरम्भ करती हैं एवं धीरे-धीरे ऊपर की पत्तियां भी सूख जाती हैं|
7. फलों वाले वृक्षों में अधिकतर फल पकने से पहले गिर जाते हैं, फलों का आकार भी छोटा रहता है, परन्तु फलों का रंग बहुत अच्छा होता है|
8. उपज व फसल गुणवत्ता खासकर शर्करा में कमी हो जाती है|
यह भी पढ़ें- कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती कैसे करें
कैल्शियम की कमी के पौधों पर लक्षण-
1. अधिक कमी होने पर नई पत्तियाँ प्रभावित होती हैं, पत्तियों का आकार छोटा एवं विकृत हो जाता है| किनारे कटे-फटे होते हैं और इनमें ऊपर ऊतक क्षय के धब्बे पाये जाते हैं तथा तने कमजोर हो जाते हैं|
2. जड़ों का विकास कैल्शियम की कमी में उचित प्रकार नहीं होता है|
3. फूलगोभी, पातगोभी और गाजर की फसलों में कैल्शियम की कमी होने पर पत्तियां छोटी रह जाती हैं, किनारे मुड़ जाते हैं और तना भी कमजोर हो जाता है|
4. आलू के पौधे झाड़ीनुमा हो जाते हैं, टयुबर का निर्माण बुरी तरह प्रभावित होता है एवं पत्ते छोटे आकार के होते हैं|
यह भी पढ़ें- जलवायु परिवर्तन, जानिए खेती एवं हमारे भविष्य पर इसके प्रभाव
जिंक की कमी के पौधों पर लक्षण-
1. तने की लम्बाई घट जाती है तथा पत्तियां मुड़ जाती है|
2. धान में जिंक की कमी को खैरा रोग के नाम से जाना जाता है, पौधों के ऊपर से तीसरी या चौथे पत्ते के पटल के बीच चॉकलेटी गहरे भूरे या लाल रंग के धब्बे बनना प्रारम्भ होते हैं|
3. गेहूं में प्रायः बुवाई के 25 से 30 दिन बाद लक्षण प्रकट होते हैं, तीसरी या चौथी पत्तियों के बीच हल्के पीले रंग के अनियमित धब्बे या धारियां दिखाई देती हैं, ये धब्बे बाद में बड़े होकर आपस में मिल जाते हैं, जिससे पूरी पत्ती सफेद, पीली या हरी चित्तियों में बदल जाती है|
4. मक्का में छोटे पौधों में जिंक की कमी से सफेद कली रोग हो जाता है, ये सफेद कलियां पौधे के मरे हुए या बेकार ऊतकों के छोटे धब्बे होते हैं|
5. जिंक की कमी से सरसों के पौधों की बढ़वार मन्द या धीमी पड़ जाती है, कमी के लक्षण बुआई के 20 दिन बाद पहली पत्ती पर आते हैं, पत्तियों के किनारे गुलाबी हो जाते हैं|
6. चने में जिंक की कमी के लक्षण पुरानी संयुक्त पत्तियों पर दिखाई देते हैं, पत्तियों की नोंक का रंग बदल जाता है|
7. मसूर में जिंक की कमी के कारण पत्तियाँ अपना हरा रंग त्याग देती है, कुछ समय बाद पत्तियों की नोंक का हल्का पीला रंग ‘V’ आकार में नीचे की ओर बढ़ता है|
यह भी पढ़ें- फ्लाई ऐश (राख) का खेती में महत्व
मैंगनीज की कमी के पौधों पर लक्षण-
1. मैंगनीज की कमी के लक्षण सबसे पहले नयी पत्तियों पर आते हैं, पत्तियों के शीर्ष से मध्य भाग की ओर अन्तःशिरा के मध्य हरिमाहीनता आ जाती है|
2. मैंगनीज की कमी का प्रथम लक्षण पत्तियों की अन्तः शिराओं में छोटे-छोटे हरिमाहीन धब्बों का विकसित होना है|
3. अनाज की फसलों में इसकी कमी से पत्तियां भूरे रंग की और पारदर्शी हो जाती है, इसके बाद ऊतक गलन रोग हो जाता है|
4. मैंगनीज की कमी से जई की भूरी चित्ती, गन्ने की अंगमारी, चुकन्दर का चित्तीदार पीला रोग, मटर का पैंक चित्ती रोग आदि उत्पन्न होते हैं|
क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी में पोषक तत्वों का उचित प्रबन्ध
क्षारीय एवं मिट्टी का उच्च पी एच मान, उच्च विनिमय योग्य सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट की अधिक मात्रा, अल्प जैव पदार्थ अंश और बंजर भूमि की खराब भौतिक दशा पोषक पदार्थों या तत्वों के रूपान्तरण तथा उनकी उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है| साधारणतया क्षारीय एवं मिट्टी में कैल्शियम और नाइट्रोजन व जिंक की कमी होती है और फास्फोरस तथा पोटाश अधिक मात्रा में होते हैं| क्षारीय मिट्टी में पोषक पदार्थो या तत्वों से सम्बन्धित कुछ मुख्य बिन्दुओं पर यहां पर प्रकाश डाला गया है जैसे-
1. इन मिट्टी में जैव पदार्थ तथा नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए प्रतिवर्ष या दो वर्ष में कम से कम एक बार हरी खाद के लिए ढेंचा अवश्य उगाएं|
2. आरम्भिक वर्षों में धान-गेहूं की फसल के लिए सामान्य मिट्टी की तुलना में क्षारीय मिट्टी में 20 से 25 प्रतिशत अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करें|
3. विनाइट्रीकरण और नाइट्रोजन का गैस के रूप में होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए 3 या 4 बार में यूरिया और अमोनियम सल्फेट 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें|
4. साधारण रूप से क्षारीय एवं मिट्टी में फास्फोरस तथा पोटाश की मात्रा अधिक होती है, तीन या चार वर्षों तक इनका प्रयोग न करने के सिफारिश की गई है| इसके पश्चात् मिट्टी परीक्षण के आधार पर केवल धान की फसल के लिए फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए|
5. धान व गेहूँ दोनों ही फसलों में दो तीन वर्षों तक 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट प्रयोग करें| बाद में मिट्टी परीक्षण के आधार पर एकान्तर वर्षों में जिंक का प्रयोग किया जा सकता है|
6. सुधारी गई चूनेदार और हल्की गठित क्षारीय मिट्टी में उगाई गई गेहूं की फसल में मैंगनीज की कमी के लक्षणों के दिखाई देने पर इसको दूर करने के लिए मिट्टी में बुवाई से पहले 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मैगनीज सल्फेट का प्रयोग करें या इसका खड़ी फसल में इसके 0.5 प्रतिशत घोल का छिड़काव करें|
7. क्षारीय एवं मिट्टी में लगातार खेती के साथ-साथ मिट्टी परीक्षण अवश्य कराएं ताकि मिट्टी की क्षारीयता का अनुमान लगाया जा सके, यदि क्षारीयता बढ़ रही है। तो पुनः जिप्सम का मिट्टी परीक्षण के आधार पर प्रयोग करें|
यह भी पढ़ें- दीमक से विभिन्न फसलों को कैसे बचाएं
क्षारीय एवं लवणीय मिट्टी में संगठित पोषक तत्व प्रबन्धन
दीर्घकालीन उर्वरक परीक्षणों के आधार पर यह पाया गया है, कि यदि लगातार रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग करने से कुछ समय के बाद फसल उत्पादन में लगातार कमी आती है| प्रयोग से यह भी प्रमाणित हुआ है, कि हरी खाद या गोबर की खाद के उपयोग से मिट्टी में नत्रजन की मात्रा बढ़ती है, तथा धीरे-धीरे फसलों की पैदावार में बढ़ोत्तरी होती है|
जिप्सम एवं गोबर की खाद द्वारा सुधारी गई क्षारीय एवं मिट्टी पर किये गये प्रयोगों से पता चलता है, कि 45 से 50 दिन के ढेंचा को मिट्टी में मिलाने से 110 किलोग्राम नत्रजन, 11 किलोग्राम फास्फोरस तथा 90 किलोग्राम पोटेशियम की मात्रा प्रति साल प्रति हेक्टेयर उपलब्ध होती है तथा इससे धान व गेहूं की फसल की पैदावार में वृद्धि देखी गई है|
दीर्घकालीन उर्वरक परीक्षणों के आधार पर पाया गया है, कि रासायनिक उर्वरकों की संस्तुति की आधी मात्रा के साथ गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर या हरी खाद के रूप में ढेचा के लगाने से जो उपज प्राप्त होती है, वह 100 प्रतिशत संस्तुति उर्वरक मात्रा की उपज के बराबर होती है| इस प्रकार धान की फसल में 50 प्रतिशत उर्वरक की मात्रा की बचत संभव है|
गोबर व ढेचा की खाद मिट्टी में मिलाने से जैविक कार्बन तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है| संगठित पोषक प्रबन्धन द्वारा संतुलित मात्रा में कार्बनिक और रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग से काफी हद तक टिकाऊपन लाया जा सकता है| इसके साथ-साथ इनके प्रयोग से जिंक की कमी को भी दूर किया जा सकता है|
यह भी पढ़ें- जड़ वाली सब्जियों के बीज का उत्पादन कैसे करें
यदि उपरोक्त जानकारी से हमारे प्रिय पाठक संतुष्ट है, तो लेख को अपने Social Media पर Like व Share जरुर करें और अन्य अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ Social Media द्वारा Facebook Page को Like, Twitter व Google+ को Follow और YouTube Channel को Subscribe कर के जुड़ सकते है|
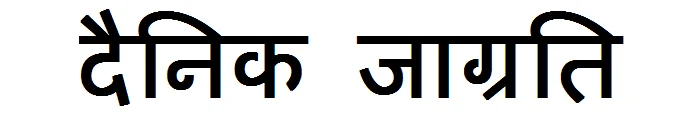
Leave a Reply