
हमारे देश में धान की खेती की जाने वाले लगभग सभी भू-भागों में भूरा पौघ माहू नीलपर्वत लूगेंस स्टाल (होमोप्टेरा डेल्फासिडै) धान का एक प्रमुख नाशककीट है| हाल में पूरे एशिया में इस कीट का प्रकोप गंभीर रूप से बढ़ा है, जिससे धान की फसल में भारी नुकसान हुआ है| ये कीट तापमान एवं नमी की एक विस्तृत सीमा को सहन कर सकते हैं|
प्रतिकूल पर्यावरण में तेजी से बढ़ सकते हैं, ज्यादा आक्रमक कीटों की उत्पती होना कीटनाशक प्रतिरोधी कीटों में वृद्धि होना, बड़े पंखों वाले कीटों का आविर्भाव तथा लंबी दूरी तय कर पाने के कारण इनका प्रकोप बढ़ रहा है| धान की वैज्ञानिक तकनीक से खेती कैसे करें, की जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें- धान (चावल) की खेती कैसे करें
भूरा पौध माहू का प्रकोप तथा वितरण
यद्यपि धान फसल में भूरा पौघ माहू सन 1900 में देखा गया, किंतु भारत में प्रथम बार व्यापक रूप से इस नाशककीट से फसल का नुकसान सन 1962 में केरल के कुट्टनाड में हुआ था| जिसके कारण बहुत आर्थिक क्षति भी हई| धान की खेती की जाने वाले राज्यों जैसे- केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा तथा पंजाब में भूरा पौघ माहू का भयंकर प्रकोप हुआ था| जिसके कारण धान की उपज में कमी हुई थी| बाद के वर्षों में भी कभी-कभी इसका प्रकोप धान की खेती पर दिखाई देता रहा है|
इन कीटों के कम प्रकोप से 10 प्रतिशत तक अनाज उपज में हानि होती है| जबकि भयंकर प्रकोप के कारण 40 प्रतिशत तक उपज में हानि होती है| खड़ी फसल में कभी-कभी अनाज का 100 प्रतिशत नुकसान हो जाता है| प्रति रोधी किस्मों और इस किट से संबंधित आधुनिक कृषिगत क्रियाओं और कीटनाशकों के प्रयोग से इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है| इस लेख में इन सब की जानकारी का उल्लेख किया गया है|
यह भी पढ़ें- धान में हरित शैवाल एवं अजोला का प्रयोग, जानिए लाभ की तकनीक
भूरा पौध माहू और संवेदनशील कारक
1. भारत में, धान की फसल साधारणतः मार्च से अप्रैल के दौरान ग्रीष्म मौसम में तथा अगस्त से अक्टूबर के दौरान आर्द्र में भूरा पौघ माहू से प्रकोपित होती है|
2. किसी क्षेत्र में लगातार धान की खेती तथा ग्राह्यशील किस्मों की खेती करने से धान की फसल मुख्यतः भूरा पौध माहू से पीड़ित होती है|
3. कम दूरी पर रोपाई करने से तथा खेत में खड़ा पानी भूरा पौध माहू कीटों की संख्या वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होता है|
4. बिना पोटैशियम या कम पोटैशियम सहित अधिक मात्रा में नत्रजन उर्वरक के प्रयोग द्वारा पौधों में कोमलता आती है, जिससे कीटों की संख्या में वृद्धि होती है तथा पौधों में उच्च प्रोटिन के कारण नाइट्रोजन माहू के जनन शक्ति में सहायक होती है|
5. अंडे एवं शिशुकीट के विकास के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है| कीट के जीवित रहने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तथा 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान प्रतिकूल परिस्थिति है|
6. भूरा पौघ माहू के विकास के लिए 40 से 75 प्रतिशत आपेक्षिक आर्द्रता अनुकूलतम है|
यह भी पढ़ें- धान के कीटों का समेकित प्रबंधन कैसे करें
भूरा पौध माहू के लक्षण और पहचान
1. यह कीट भूरा रंग का, आकार में छोटा है, यह फुदकता है और कूदता है| चूंकि ये कीट पौधों के मूल में पानी के सतह से थोड़ा सा ऊपर पत्तों के घने छतरी के नीचे रहते हैं, किसानों को इन कीटों के बारे में शीघ्र पता नहीं लग पाता है तथा इनका नियंत्रण उपाय अधिक जटिल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रबंधन प्रणाली जटिल हो जाती है|
2. मादा कीट पौधे के निचले तरफ (पत्ता आच्छद) में 40 से 200 अंडे देती है| यह छेद करती है और पर्ण आच्छद के भीतर अंडों को घुसा देती है| इस छेदन को तना के बाहर से एक भूरे धब्बे के रूप में स्पष्ट देखा जा सकता है|
3. अंडनिक्षेपण के 4 से 10 दिन के बाद अंडों का स्फुटन होता है| कीट अपने विकास अवधि के दौरान पांच अर्भकीय इंस्टार से गुजरती हैं| साधारणतया कीट सफेद से भूरे रंग में बदल जाते हैं|
4. अर्भकीय विकास में लगभग 12 से 14 दिन लगते हैं, और कीट भूरा या सफेद वयस्क हो जाता हैं| सामान्य परिस्थिति में नर और मादा दोनों पंखरहित (ब्रेकिप्टरोस) होते हैं तथा भूरा पौध माहू वयस्क होने के 2 से 3 दिन बाद मादा अंडे देना आंरभ करती हैं| जब एक फसल क्षेत्र में कीट संख्या अधिक हो जाती है, तब पंखदार (माक्रोप्टेरोस) कीट स्थान बदलती हैं और नए फसल क्षेत्रों को प्रकोपित करती है| रोपाई करने के 50 से 60 दिन बाद इनकी संख्या सर्वाधिक हो जाती हैं या कटाई के आरंभ अवस्था में अत्यधिक होती हैं| प्रत्येक पौध पूंजा के मूल में मादा कीट लगभग 200 से 500 अंडे देती हैं|
यह भी पढ़ें- धान में एकीकृत रोग प्रबंधन कैसे करें
पौधों में भूरा पौध माहू संक्रमण
1. ये कीटें पौधों के मूल में पानी के सतह से थोड़ा सा उपर रहती हैं|
2. भूरा पौध माहू धान पौधों से तरल पदार्थ एवं पौषक तत्व लगातार चूसते हैं जिसके कारण आरंभ में पौधे पीले हो जाते हैं|
3. पौधों पर पीलापन एवं भूरापन होता है तथा वे धीरे-धीरे सुख जाते हैं| फसल नुकसान के इस लक्षण को हापर बर्न के नाम से जाना जाता है|
4. पौध के मूल में संक्रमित स्थानों पर हॉनीड्यू तथा फफूंद दिखाई देते हैं|
5. इस कीट से एक रोग भी फैलता है, जिसे ग्रासी स्टंट रोग कहा जाता हैं, जिससे पत्ते पीले हो जाते हैं और पौधों की वृद्धि कम होती है|
भूरा पौध माहू का समन्वित रोकथाम
1. समन्वित कीट रोकथाम पद्धति सर्वोत्तम नाशककीट प्रबंधन रणनीति प्रदान करता है तथा किसानों की आर्थिक एवं उपलब्ध संसाधन पर करता है| रोकथाम कार्यकलापो को असरदार बनाने के लिए लगातार निगरानी की आवश्यकता है|
2. उपलब्धता के आधार पर बिन-रासायनिक पद्धति अपनाना चाहिए क्योंकि इससे बिना किसी खर्च के साथ-साथ प्रयोगकर्ता एवं पर्यावरण के लिए सुरक्षित है|
3. अंतिम विकल्प के रूप में रासायनिक नियंत्रण का प्रयोग करना चाहिए तथा प्रयोग करते समय चेहरा मास्क तथा हस्त मास्क पहनना चाहिए और प्रयोग करने के बाद कीटनाशक पात्रों का सुरक्षित तरीके से निपटान करना चाहिए|
4. फसल के मूल की ओर पर्णीय छिड़काव करना चाहिए तथा कीटों की संख्या को देखकर 7 से 10 दिनों के बाद इसका प्रयोग दोहराना चाहिए| हाथों से छिड़काव किये जाने वाले पर्णीय छिड़काव की मात्रा 500 लीटर प्रति हेक्टेयर तथा शक्तिचालित छिड़काव के मामले में इसकी मात्रा 200 लीटर प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए|
5. फोस्फोमाइडन, फोरेट, मिथाइल पाराथियन तथा सिंथेटिक पाइरिथ्राएड्स जैसे कीटनाशकों के प्रयोग मत करें, क्योंकि अध्ययन से पता चला है कि इन रसायनों के प्रयोग से कीटों का नियंत्रण नहीं हो पाता है|
यह भी पढ़ें- असिंचित क्षेत्रों में धान की फसल के कीट एवं उनका प्रबंधन कैसे करें
भूरा पौध माहू पर नियंत्रण के उपाय
पारंपरिक पद्धति-
1. कीट पीड़ित खेतों से जल निकासी, उर्वरक का उचित मात्रा में प्रयोग, नत्रजन उर्वरक का भागों में प्रयोग आदि को अपनाने पर भूरा पौध माहू की संख्या में कमी होती है|
2. अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक 8 या 10 पंक्तियों के बाद मार्ग निर्माण से कीटों की संख्या को कम करने में सहायता मिलती है तथा अत्यधिक जरूरी परिस्थिति में कीटनाशकों का छिड़काव करने में भी सुविधा होती है| धान की खेती में कीट प्रकोप पर निगरानी रखना अत्यंत जरूरी है|
3. संवेदनशील किस्म की खेती उसी क्षेत्र में लगातार नहीं करनी चाहिए| उनके स्थान पर प्रतिरोधी या सहिष्णु किस्मों या धान के अतिरिक्त किसी अन्य फसल की खेती करनी चाहिए|
यह भी पढ़ें- धान में खरपतवार एवं निराई प्रबंधन कैसे करें
प्रतिरोधी या सहिष्णु किस्मों की खेती-
प्रतिरोधी अथवा सहिष्णु किस्मों की खेती भूरा पौध माहू रोकथाम प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है| कई लोकप्रिय किस्में इस नाशककीट के प्रति सहिष्णु या प्रतिरोधी पाई गईं हैं, जैसे- उदय, दया, ललाट, शक्तिमान (ओडिशा) ज्योति, भद्र, कार्तिक, मेकोन, रेम्या, कनक (केरल), भारतीदसन (पांडिचेरी), आंध्र प्रदेश में सोनासाली, नागार्जुन, वज्रम, तथा किशनवेणी, मानसरोवर (केंद्रीय विमोचन) आदि| विभिन्न राज्यों के भूरा पौध माहू द्वारा अत्यधिक प्रभावित पीड़ित क्षेत्रों में इन धान की किस्मों की खेती की जानी चाहिए|
शिकारी या परभक्षी-
स्वस्थाने प्राकृतिक शत्रुओं के संरक्षण से विशेषकर शिकारी मकड़ी, लाइकोसा सुडोआनुलटा तथा आरजिओप एस पी से पौध माहू का असरदार नियंत्रण हो सकता है| अंडा खाने वाला एक प्रमुख शिकारी कीट सिझेनिस लिविडपानिस रयटर से भी नियंत्रण हो सकता है|
वानस्पतिक नियंत्रण-
1. धान की खेती में जब 3 से 5 कीट प्रति पूंजा हो जाएं तब वानस्पतिकों का प्रयोग करना चाहिए|
2. नीम तेल तथा कुछ नीम आधारित रसायनों जैसे नेथ्रिन, निंबीसाइडिन तथा नीमगोल्ड का 5 से 6 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर में 0.5 मिलीलीटर तरल डिटरजेंट के साथ मिलाकर पर्णीय छिड़काव करने से धान की खेती में कीट संख्या कम हो सकती है|
3. आजाडिराक्टीन 5 प्रतिशत डब्ब्ल्यू/डब्ल्यू तथा नीम निचोड़ गाढा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जा सकता है| जलमिर्च (पोलिगोनुम हाइड्रोपाइपर) के निचोड़ का 20 ग्राम प्रति लीटर की दर से 0.5 मिलीलीटर तरल डिटरजेंट के साथ मिलाकर प्रयोग करने पर भूरा पौध माहू कीटें मर जाती हैं|
4. नीम तेल या उपरोक्त नीम आधारित रसायनों का कीटनाशकों की आधी मात्रा के साथ मिलाकर धान की खेती में प्रयोग करने से कीटों का नियंत्रण हो सकता है|
यह भी पढ़ें- सिंचित क्षेत्रों में धान की फसल के कीट एवं उनका प्रबंधन कैसे करें
रासायनिक नियंत्रण-
1. धान की खेती में जब कीटों की संख्या 5 से 10 कीट प्रति पूंजा हो जाती है, तब फसल में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए|
2. कम मात्रा में उच्च क्षमता के कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोप्रिड, थियोमेथोक्साम का 125 मिलीलीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से तथा इथोफेनफ्राक्स, फिप्रोनील की 1000 मिलीलीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जा सकता है| जबकि क्लोथियानीदीन 10 से 12 ग्राम प्रति हैक्टर की दर से प्रयोग किया जा सकता है|
3. साधारण रूप से प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों जैसे क्लोरोपाइरीफस, की 1.5 लीटर प्रति हैक्टर मात्रा, पर्णीय छिड़काव के रूप में तथा कार्बोफ्यूरान दानेदार 33 किलोग्राम प्रति हैक्टर दर पर प्रयोग करने से इस नाशककीट का नियंत्रण अच्छी तरह किया जा सकता है|
यह भी पढ़ें- धान में सूत्रकृमि एवं प्रबंधन कैसे करें
यदि उपरोक्त जानकारी से हमारे प्रिय पाठक संतुष्ट है, तो लेख को अपने Social Media पर Like व Share जरुर करें और अन्य अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ Social Media द्वारा Facebook Page को Like, Twitter व Google+ को Follow और YouTube Channel को Subscribe कर के जुड़ सकते है|
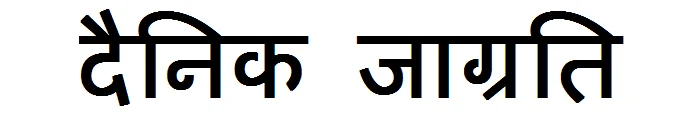
Leave a Reply