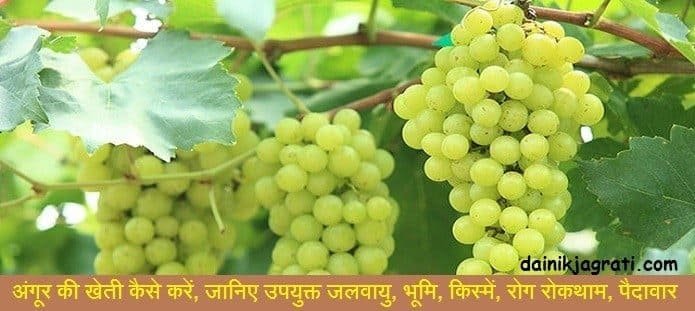
अंगूर की बागवानी लगभग पूरे भारतवर्ष में सभी क्षेत्रों में की जा सकती है| अंगूर के फल स्वादिष्ट तथा स्वास्थ्य के हितकारी होने के कारण इसकी बागवानी की महत्ता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है| पिछले दो से तीन वर्षों में इसके क्षेत्रफल में काफी तेजी के साथ बढ़ोत्तरी हुई है| उत्पादन के आधार पर दक्षिण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु मुख्य राज्य हैं| जबकि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली राज्यों में इसकी बागवानी की जा रही है|
पिछले दशक में उत्तर भारत में अंगूर के उत्पादन क्षेत्र में गिरावट देखी गई जिसके कई कारण प्रमुख हैं, जैसे त्रुटियुक्त कांट-छांट, कुपोषण एवं सूक्ष्म तत्वों की कमी, क्षारीय भूमि का फैलाव, मूलवृंतों का न के बराबर प्रयोग, दीमक की समस्या इत्यादि| उत्तर भारत में अंगूर की फसल वर्ष में केवल एक बार जून में ली जाती है, जबकि दक्षिण भारत में दो बार ली जाती है| इसकी बेल शीघ्र बढ़ने वाली होती है तथा तीसरे वर्ष से फल देने योग्य हो जाती है|
लेकिन यह तभी संभव हो सकता है, यदि पौधों की प्रारम्भिक अवस्था से ही उचित ढंग से देख रेख की गई हो| उत्तर भारत में अंगूर की सफल बागवानी के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनानी होगी ताकि इसकी फसल से लगातार अच्छा उत्पादन प्राप्त होता रहे| इस लेख में कृषकों के लिए अंगूर की वैज्ञानिक तकनीक से खेती कैसे करें की जानकारी का उल्लेख किया गया है|
यह भी पढ़ें- नींबू की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार
उपयुक्त जलवायु
अंगूर की खेती के लिए गर्म, शुष्क, तथा दीर्घ ग्रीष्म ऋतू अनुकूल रहती है| लेकिन बहुत अधिक तापमान हानी पहुंचा सकता है, अधिक तापमान के साथ अधिक आद्रता होने से रोग लग जाते है| जलवायु का फल के विकास तथा पके हुए अंगूर की बनावट और गुणों पर काफी असर पड़ता है| अंगूर के पकते समय वर्षा या बादल का होना बहुत ही हानिकारक है| इससे फल फट जाते हैं और फलों की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पड़ता है| अतः उत्तर भारत में जल्दी पकने वाली किस्मों की सिफारिश की जाती है|
भूमि का चयन
अंगूर की खेती या बागवानी अनेक प्रकार की मृदा में कि जा सकती है| अंगूर की जड़ की संरचना काफी मजबूत होती है| अतः यह कंकरीली,रेतीली से चिकनी तथा उथली से लेकर गहरी मिट्टियों में सफलतापूर्वक पनपता है| लेकिन रेतीली, दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकास अच्छा हो अंगूर की खेती के लिए उत्तम पाई गयी है| अधिक चिकनी मिट्टी में इसकी खेती न करे तो बेहतर है| अंगूर लवणता के प्रति कुछ हद तक सहनशील है|
यह भी पढ़ें- कागजी नींबू की खेती कैसे करें
उन्नत किस्में
उत्तर भारत में उगाए जाने वाली किस्मों के चयन एवं उनके विकास व विस्तार में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने विशेष योगदान दिया है| इसमें किस्मों का विकास, सस्य तकनीकों का मानकीकरण, वृद्धि नियामकों का उपयोग, आदि भी शामिल हैं| उपोष्ण क्षेत्रों में उगाए जाने वाली कुछ प्रचलित और उन्नत किस्में इस प्रकार है, जैसे- ब्युटी सीडलेस, परलेट, पूसा सीडलेस, पूसा उर्वशी, पूसा नवरंग और फ्लैट सीडलेस आदि प्रमुख है| किस्मों की विस्तार से जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें- अंगूर की उन्नत किस्में
प्रवर्धन तकनीक
अंगूर की खेती हेतु प्रवर्धन मुख्यतः कटिंग कलम द्वारा होता है| जनवरी माह में काट छाँट से निकली टहनियों से कलमे ली जाती हैं| कलमे सदैव स्वस्थ और परिपक्व टहनियों से ही ली जाने चाहिए| सामान्यतः 4 से 6 गांठों वाली 25 से 45 सैंटीमीटर लम्बी कलमें ली जाती हैं| कलम बनाते समय यह ध्यान रखें कि कलम का निचे का कट गांठ के ठीक नीचे होना चाहिए और ऊपर का कट तिरछा होना चाहिए| इन कलमों को अच्छी प्रकार से तैयार की गयी तथा जमीन की सतह से ऊँची क्यारियों में लगा देते हैं| एक वर्ष पुरानी जड़युक्त कलमों को जनवरी माह में नर्सरी से निकल कर खेत में रोपित कर देते हैं| अंगूर प्रवर्धन की विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें- अंगूर का प्रवर्धन कैसे करें
गड्ढ़े की तैयारी
अंगूर की बागवानी के लिए करीब 50 x 50 x 50 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदकर उसमें सड़ी गोबर की खाद (15 किलोग्राम), 250 ग्राम नीम की खली, 50 ग्राम फॉलीडाल कीटनाशक चूर्ण, 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट व 100 ग्राम पोटेशियम सल्फेट प्रति गड्ढे मिलाकर भर दें| पौध लगाने के करीब 15 दिन पूर्व इन गड्ढ़ों में पानी भर दें ताकि वे तैयार हो जाएं| जनवरी माह में इन गड्ढों में 1 साल पुरानी जड़वाली कलमों को रोप दें| पौध लगाने के बाद तुरन्त सिंचाई करना आवश्यक है|
यह भी पढ़ें- संतरे की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार
खाद और उर्वरक
अंगूर की खेती को काफी मात्र में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है| अतः खेत की भूमि कि उर्वरता बनाये रखने के लिए और लगातार अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लेने के लिए, यह आवश्यक है, की खाद और उर्वरकों द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति की जाये। अंगूर की आदर्श विधि 3 x 3 मीटर की दुरी पर लगाई गयी अंगूर की 5 वर्ष या आगे के वर्षों हेतु बेल में लगभग 600 ग्राम नाइट्रोजन, 750 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 650 ग्राम पोटेशियम सल्फेट और 60 से 70 किलोग्राम गोबर की खाद की आवश्यकता होती है|
छंटाई के तुंरत बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में नाइट्रोजन और पोटाश की आधी मात्रा व फास्फोरस की पूरी मात्रा डाल देनी चाहिए| शेष मात्रा फल लगने के बाद दें| खाद और उर्वरकों को अच्छी तरह मिट्टी में मिलाने के बाद तुंरत सिंचाई करें| खाद को मुख्य तने से दूर 20 से 25 सैंटीमीटर की दुरी से डालें|
| लता की आयु (वर्ष) | गोबर की खाद (किलोग्राम) | नाइट्रोजन (ग्राम) | फास्फेट (ग्राम) | पोटाश (ग्राम) |
| पहला | 15 | 150 | 125 | 150 |
| दूसरा | 30 | 300 | 250 | 300 |
| तीसरा | 45 | 400 | 375 | 450 |
| चौथा | 60 | 500 | 500 | 650 |
| पाचवां व आगे | 70 | 600 | 650 | 750 |
यह भी पढ़ें- किन्नू की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार
सिंचाई प्रबंधन
अंगूर की खेती में सिंचाई लता के फलत के समय अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है| इस समय मृदा में नमी कि कमी का हानिकारक प्रभाव पड़ता है और फलो का आकार और गुणवत्ता घट जाती है| फलो के पकने के समय जलाभाव से अंगूरों के गुच्छे का रंग चमकीला रहता है, फिर भी जब फल पकने को होते है, उस समय नमी थोड़ी भी कमी होने से परिपक्वता जल्दी आ जाती है|
लेकिन फलो को तोड़ने के समय सिंचाई, यदि अधिक कि जाती है, तो फलो का आकार तो बढ़ जाता है| लेकिन गुणवत्ता घट जाती है और भंडारण शक्ति भी कम हो जाती है| इसलिए सिंचाई तापमान और पर्यावरण स्थितियों को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए अर्थात छंटाई एवं खाद डालने के तुरन्त बाद और जब पौधे फुटाव लेने लगें तो सिंचाई करना अति आवश्यक है|
गर्मी के मौसम में लगातार एक सप्ताह के अन्तराल पर सिंचाई करें| जून के महीने में अधिक गर्मी पड़ने के कारण नए पौधों की सप्ताह में दो बार सिंचाई करनी चाहिए| नवम्बर से जनवरी तक बेलों की सुषुप्तावस्था के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए| इसके अतिरिक्त बरसात के महीनों में यदि वर्षा न हो तो सिंचाई प्रत्येक सप्ताह करें|
यह भी पढ़ें- बागवानी पौधशाला (नर्सरी) की स्थापना करना, देखभाल और प्रबंधन
कटाई-छटाई एवं सधाई
अंगूर की खेती से अच्छे उत्पादन में कटाई-छटाई का बड़ा महत्व है| कटाई-छटाई के दो उद्देश्य होते है| पहला लता कि समुचित ढ़ंग से किस्म कि ओज क्षमता के अनुसार सधाई करना तथा एक स्थाई ढ़ांचा निर्मित करना ताकि लता का विकास चारों दिशाओं में समुचित रूप से हो सके और दूसरा लताओं से नियमित रूप से फल प्राप्त करना इसलिए प्रथम दो वर्षों के अन्दर लता को ढ़ांचा प्रदान किया जाता है|
अंगूर कि सधाई कि अनेक विधियां है और इनके अलग-अलग गुण दोष है परन्तु उत्तर भारत में अंगूर कि सधाई कि तीन से चार मुख्य प्रचलित विधियां है, जैसे- शीर्ष प्रणाली, जाफर प्रणाली और पंडाल प्रणाली आदि| अंगूर के बागों की कटाई-छटाई एवं सधाई की सम्पूर्ण जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें- अंगूर के पौधों की काट-छांट एवं सधाई कैसे करें
निकाई-गुड़ाई
मुख्यतः बरसात में खरपतवार अधिक उगते हैं और तेजी से बढ़ते हैं| इसके कारण बेलों की बढ़वार रूक जाती है और पौधे कमजोर हो जाते हैं| इसके साथ-साथ बेलों में आर्द्रता बढ़ती है, जिससे बीमारियों को बढ़ावा और हानिकारक कीटों को सुरक्षा मिलती है| इसलिए बेलों में खरपतवारों को न बढ़ने दें और समय-समय पर निकाई-गुड़ाई करके निकालते रहें|
खरपतवारों को कुछ रसायनों द्वारा भी नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे डियुरिन 3 किलोग्राम या सिमेजीन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अगस्त और फरवरी के महीने में घास उगने से पहले भूमि में डाल दें| इसके अतिरिक्त उगी हुई घास को जलाकर नष्ट करने के लिए ग्रामेक्सोन का छिड़काव सितम्बर व मार्च के महीनों में करें|
परन्तु इस सावधानी के साथ कि यह बेलों की पत्तियों, शाखाओं और तने पर नहीं पड़े| बरसात के बाद बेलों की दो बार गुड़ाई कर दें| छंटाई व खाद डालने के तरुन्त बाद गुड़ाई करना अतिआवश्यक है| इसके अतिरिक्त खरपतवार होने पर एवं सिंचाई के बाद आवश्यकनुसार समय-समय पर निकाई-गुड़ाई करते रहना चाहिए|
यह भी पढ़ें- लीची की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार
गुणवत्ता में सुधार
जनवरी के प्रथम सप्ताह में छंटाई के तुरन्त बाद बेलों पर डॉर्मेक्स या डॉरब्रेक (30 ए आई) का 1.5 प्रतिशत घोल का छिड़काव फूल आने व फल पकने में करीब दो सप्ताह तक अगेता हो जाता है| थायोयुरिया (2 प्रतिशत) का छिड़काव करने पर भी 10 से 12 दिन पहले फल पक कर तैयार हो जाते हैं| इन विनियामकों के उपयोग से फलों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है| अंगूर के दानों की लम्बाई बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है|
ब्यूटी सीडलेस किस्म में 45 पी पी एम व परलेट, पूसा उर्वशी और पूसा सीडलेस में 25 से 30 पी पी एम, जी ए 3 घोल का अनुकूलन प्रभाव देखा गया है| जी ए 3 के घोल को प्लास्टिक के मग में लेकर, 50 प्रतिशत, फूल खिलने पर व दाने बनने के बाद दो बार उपचार करते हैं| फल के रंग एवं मिठास में सुधार के लिए फल जब पकने से करीब एक महीने पहले इश्रेल 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में गुच्छों को डुबोना चाहिए|
छल्ला विधि से तना के किसी भाग पर 0.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की छाल उतार ली जाती है| पकने के समय छल्ला उतारने पर दानों के रंग एवं मिठास में सुधार लाया जा सकता है| इसके साथ कई किस्मों में गुच्छों की सघनता कम करके दानों के आकार में बढ़ोत्तरी की जा सकती है| फूल आने पर ब्रुश द्वारा प्रति गुच्छा फूलों की मात्रा को कम करके भी दाने के आकार में सुधार लाया जा सकता है|
यह भी पढ़ें- अमरूद की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार
रोग एवं रोकथाम
उत्तरी भारत में अंगूर की बेलों पर बरसात के आरम्भ होते ही विशेषकर एन्ट्रेक्नोज, सफेद चूर्णिल रोग तथा सरकोस्पोरा पत्ती धब्बा बीमारियों को प्रकोप होता है| एन्छेक्नोज का आक्रमण बरसात व गर्मी (जून से जुलाई) के साथ-साथ आरम्भ हो जाता है तथा यह बहुत तेजी से फैलता है| इससे पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जो बीच में दबे होते हैं|
धब्बे फैलकर टहनियों पर आ जाते हैं| सरकोस्पोरा पत्ती धब्बा के धब्बे गोल और इनका रंग सिरों पर लाल-भूरा व बीच में तूडें जैसा होता है| एन्ट्रेक्नोज एवं सरकोस्पोरा के आक्रमण से पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं और टहनियां भी पूरी तरह से सूख जाती हैं| कभी-कभी तो पूरी बेल ही सूख जाती है|
रोकथाम-
एन्छेक्नोज एवं सरकोस्पोरा पत्ती धब्बा की बीमारियों की रोकथाम के लिए ब्लाईटाक्स या फाइटालोन का 0.3 प्रतिशत का छिड़काव अर्थात 750 ग्राम 250 लीटर पानी में प्रति एकड़ की मात्रा से एक बार जून के अन्तिम सप्ताह में करें और 15 दिनों के अन्तराल पर सितम्बर तक करते रहें|
एन्छेक्नोज हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड (0.2 प्रतिशत) या बाविस्टीन (0.2 प्रतिशत) का छिड़काव करें| बादल छाये रहने पर 7 से 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव जरूरी है|
सफेद चूर्णिल रोग शुष्क जलवायु में देखा जाता है| इसके नियंत्रण के लिए 0.2 प्रतिशत घुलनशील गंधक या 0.1 प्रतिशत कैराथेन या 3 ग्राम प्रति लीटर पानी बाविस्टीन का छिड़काव दो बार 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए|
यह भी पढ़ें- पपीते की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार
कीट एवं रोकथाम
पत्ते खाने वाली चैफर बीटल अंगूर की बेलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों में सबसे अधिक खतरनाक है| चैफर बीटल दिन के समय छिपी रहती है तथा रात में पत्तियां खाकर छलनी कर देती है| बालों वाली सुंडियां मुख्यत: नई बेलों की पत्तियों को ही खाती हैं| इनके साथ-साथ स्केल कीट, जो सफेद रंग का बहुत छोटा एवं पतला कीड़ा होता है, टहनियों शाखाओं तथा तने पर चिपका रहता है और रस चूसकर बेलों को बिलकुल सुखा देता है| इनके अतिरिक्त एक बहुत छोटा कीट थ्रिप्स है, जोकि पत्तियों की निचली सतह पर रहता है| थ्रिप्स पत्तियों का रस चूसता है| इससे पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं और वे पीली पड़कर गिर जाती हैं|
रोकथाम-
उपरोक्त कीटों के प्रकोप से बेलों को बचाने के लिए बी एच सी (10 प्रतिशत) का धूड़ा 38 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अथवा फोलिथियोन या मैलाथियोन या डायाजिनान का 0.05 प्रतिशत से 0.1 प्रतिशत का छिड़काव जून के अन्तिम सप्ताह में करना चाहिए और बाद में छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर जुलाई से सितम्बर तक करते रहें| इसके अतिरिक्त स्केल कीट के प्रकोप से बेलों को बचाने के लिए छंटाई करने के तुरन्त बाद 0.1 प्रतिशत वाले डायाजिनान का एक छिड़काव करना आवश्यक है|
अन्य नाशीजीव अंगूर में पत्ती लपेटक इल्लियां काफी नुकसान पहुंचाती है| इसके नियंत्रण हेतु 2 मिलीलीटर मैलाथियान या डाइमेथोएट प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है| दीमक से बचने के लिए 15 से 20 दिन के अंतराल पर 5 प्रतिशत क्लोरोपाइरीफोस घोल से सिंचाई करके बेलों को बचाया जा सकता है|
यह भी पढ़ें- आम की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार
जल निकास
अंगूर की बेलों में पानी अधिक समय तक खड़ा रहना इसकी बागवानी के लिए बहुत हानिकारक होता है| पानी के लगातार खड़ा रहने से इसकी जड़ें गल जाती हैं और बेलें सूख जाती हैं| इसलिए बरसात के फालतू पानी को बाहर निकालने के लिए जून माह में जल-निकास नालियां तैयारी करनी चाहिए|
फलों की तुड़ाई
अंगूर में गुच्छों के पूर्णरूप से पक जाने पर ही तुड़ाई करनी चाहिए| जब दाने खाने योग्य या उनकी बाह्य सतह मुलायम हो जाए, तब तोड़ा जाना चाहिए| फलों की तुड़ाई प्रात: या सायंकाल में करनी चाहिए, ताकि तुड़ाई के बाद उन्हें ग्रेड कर पैकिंग की जा सके दिन में तोड़े फलों को दो घण्टे छाया में छोड़ना चाहिए|
पैदावार
भारत में अंगूर की औसत पैदावार 30 टन प्रति हेक्टेयर है, जो विश्व में सर्वाधिक है| वैसे तो पैदावार किस्म, मिट्टी और जलवायु पर निर्भर होती है, लेकिन उपरोक्त वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने पर एक पूर्ण विकसित बाग से अंगूर की 30 से 50 टन पैदावार प्राप्त हो जाती है|
यह भी पढ़ें- केले की खेती कैसे करें, जानिए किस्में, देखभाल और पैदावार
यदि उपरोक्त जानकारी से हमारे प्रिय पाठक संतुष्ट है, तो लेख को अपने Social Media पर Like व Share जरुर करें और अन्य अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ Social Media द्वारा Facebook Page को Like, Twitter व Google+ को Follow और YouTube Channel को Subscribe कर के जुड़ सकते है|
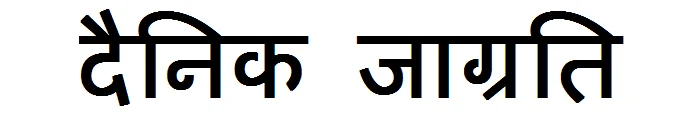
Leave a Reply