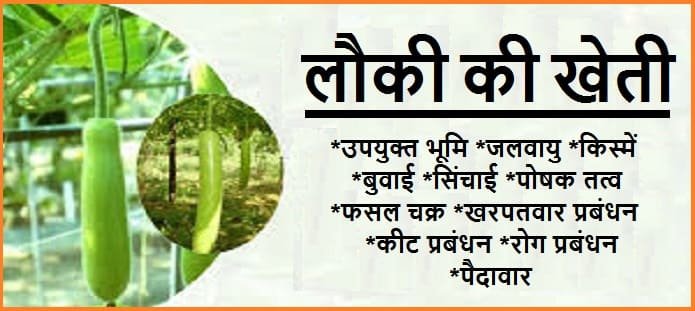
सब्जियों में घिया (लौकी) एक कद्दूवर्गीय महत्वपूर्ण सब्जी है| लौकी (Gourd) की खेती से प्राप्त फल को विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे- रायता, कोफ्ता, हलवा, खीर इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग करते हैं| यह कब्ज को कम करने, पेट को साफ करने, खाँसी या बलगम दूर करने में अत्यन्त लाभकारी है| इसके मुलायम फलों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खाद्य रेशा, खनिज लवण के अलावा प्रचुर मात्रा में अनेकों विटामिन पाये जाते हैं| लौकी की खेती पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक विस्तृत रूप में की जाती है|
निर्यात की दृष्टि से सब्जियों में घिया (लौकी) अत्यन्त महत्वपूर्ण है| किसानों को चाहिए की वो इसकी परम्परागत तरीके से खेती न करके वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करें| जिससे उनको अधिकतम पैदावार प्राप्त हो सके| इस लेख में घिया (लौकी) की वैज्ञानिक तकनीक से खेती कैसे करें का उल्लेख किया गया है| घिया (लौकी) की जैविक तकनीक से उन्नत खेती की जानकारी यहाँ पढ़े- लौकी की जैविक खेती: किस्में, देखभाल और पैदावार
लौकी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु
घिया (लौकी) की अच्छी उपज के लिए गर्म और मध्यम आर्द्रता वाले भौगोलिक क्षेत्र सर्वोत्तम होते हैं| इसलिए इसकी फसल जायद तथा खरीफ दोनों ऋतुओं में सफलतापूर्वक उगायी जा सकती है| बीज अंकुरण के लिए 30 से 35 डिग्री सेन्टीग्रेड तथा पौधों की बढ़वार के लिए 32 से 38 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान उत्तम होता है|
लौकी की खेती के लिए भूमि का चयन
बलुई दोमट और जीवांश युक्त चिकनी मिट्टी जिसमें जल धारण क्षमता अधिक तथा पी एच मान 6.0 से 7.0 हो घिया (लौकी) की खेती के लिए उपयुक्त होती है| पथरीली या ऐसी भूमि जहाँ पानी खड़ा होता हो तथा जल निकास का अच्छा प्रबन्ध न हो इसकी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है|
यह भी पढ़ें- कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती कैसे करें
लौकी की खेती के लिए भूमि की तैयारी
घिया (लौकी) की खेती हेतु खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और बाद में 2 से 3 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करते हैं| प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी और समतल कर लेना चाहिए, जिससे खेत में सिंचाई करते समय पानी कम या ज्यादा न लगे|
लौकी की खेती के लिए उन्नत किस्में
कृषकों को किस्मों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए| घिया (लौकी) की दो प्रकार की एक लम्बी बेलनाकार और दूसरी गोल गोलाकार प्रकार की किस्में होती है| कुछ उन्नत और संकर किस्मों का वर्णन इस प्रकार है, जैसे-
काशी गंगा- इस किस्म के पौधे मध्यम बढ़वार वाले और तनों पर गाँठे कम दूरी पर विकसित होती हैं| फल मध्यम लम्बा 30.0 सेंटीमीटर व फल का व्यास कम 6.90 सेंटीमीटर होता है| प्रत्येक फल का औसत भार 800 से 900 ग्राम होता है| गर्मी के मौसम में 50 दिनों बाद तथा बरसात में 55 दिनों बाद फलों की प्रथम तुड़ाई की जा सकती है| इस घिया (लौकी) प्रजाति की औसत उत्पादन क्षमता 44 टन प्रति हेक्टेयर है|
काशी बहार- इस संकर किस्म में फल पौधे के प्रारम्भिक गाँठों से बनने प्रारम्भ होते हैं| फल हल्के हरे, सीधे, 30 से 32 सेंटीमीटर लम्बे 780 से 850 ग्राम वजन वाले और 7.89 सेंटीमीटर व्यास वाले होते हैं। इसकी औसत पैदावार 52 टन प्रति हेक्टेयर है| गर्मी तथा बरसात दोनों ऋतुओं के लिए उपयुक्त किस्म है| यह किस्म नदियों के किनारे उगाने के लिए भी उपयुक्त है|
पूसा नवीन- इस किस्म के फल बेलनाकार, सीधे तथा लगभग 550 ग्राम के होते हैं| घिया (लौकी) इस किस्म की उत्पादन क्षमता 35 से 40 टन प्रति हेक्टेयर है|
अर्को बहार- इस घिया (लौकी) किस्म के फल सीधे, मध्यम आकार के लगभग 1 किलोग्राम वजन के होते हैं| फल हल्के हरे रंग के होते हैं, इसकी उत्पादन क्षमता 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है|
यह भी पढ़ें- कद्दू वर्गीय फसलों के संकर बीज का उत्पादन कैसे करें
नरेन्द्र रश्मि- फल हल्के हरे तथा छोटे-छोटे होते हैं| फलों का औसतन वजन 1 किलोग्राम होता है| इस किस्म की औसत पैदावार 30 टन प्रति हेक्टेयर है| पौधों पर चूर्णिल व मृदुरोमिल आसिता का प्रकोप कम होता है|
पूसा सन्देश- पौधे मध्यम लम्बाई के और गाँठों पर शाखाएं कम दूरी पर विकसित होती हैं| फल गोलाकार, मध्यम आकार के वे लगभग 600 ग्राम वजन के होते हैं| बरसात वाली फसल 55 से 60 दिनों व गर्मी वाली फसल 60 से 65 दिनों बाद फल की प्रथम तुड़ाई की जा सकती है| औसत पैदावार 32 टन प्रति हेक्टेयर है|
पूसा समर प्रोलिफिक राउंड- इसके फल गोलाकार हरे रंग के होते है| इसकी पैदावार 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है|
पूसा कोमल- इसके फल लम्बे होते है| यह घिया (लौकी) की अगेती किस्म है, 70 दिन में फल तोड़ने लायक हो जाते है| इसकी पैदावार 450 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है|
पूसा हाइब्रिड 3- यह घिया (लौकी) की अगेती संकर किस्म है| इसके फल लम्बे गोल होते है| यह पैदावार के लिए अच्छी किस्म है|
उत्तरा- घिया (लौकी) की इस किस्म के फल 55 से 60 दिन में तोड़ने योग्य हो जाते है| फल लम्बे और एक समान होते है|
इनके अतिरिक्त भी घिया (लौकी) की अन्य किस्में है, जैसे- स्वाती, लट्टू न- 17, पूसा संतुष्टि, प्रोलिफिक लोंग, पंजाब राउंड, पंजाब कोमल, पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत कल्यानपुर हरी लम्बी, आजाद हरित और आजाद नूतन प्रमुख है|
लौकी की खेती के लिए खाद और उर्वरक
घिया (लौकी) की फसल के लिए जुताई के समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की गली सड़ी खाद डालनी चाहिए| साथ में अच्छी पैदावार के लिए पोषण के रूप में 50 से 70 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए|
नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय देना चाहिए| बची हुई नत्रजन की आधी मात्रा दो समान भागों में बाँटकर 4 से 5 पत्ती की अवस्था तथा शेष आधी मात्रा पौधों में फूल बनने के पहले टाप ड्रेसिंग के रूप में देनी चाहिए|
यह भी पढ़ें- कद्दूवर्गीय सब्जी की फसलों में समेकित नाशीजीव प्रबंधन
लौकी की खेती के लिए बीज की मात्रा
घिया (लौकी) की सीधी बीज बुआई के लिए 2.5 से 3 किलोग्राम बीज एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त होता है, परन्तु पालीथीन के थैलों या नियंत्रित वातावरण युक्त गृहों में (प्रो ट्रे) नर्सरी उत्पादन करने के लिए 1 किलोग्राम बीज ही पर्याप्त होता है|
लौकी की खेती के लिए बुआई का समय
घिया (लौकी) की बुआई ग्रीष्म ऋतु (जायद) में 15 से 25 फरवरी तक और वर्षा ऋतु (खरीफ) में 15 जून से 15 जुलाई तक कर सकते हैं| पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई मार्च से अप्रैल के महीने में की जाती है|
लौकी की खेती के लिए बुआई की विधि
घिया (लौकी) की बुआई के लिए गर्मी के मौसम में 2.5 से 3.5 व वर्षा के मौसम में 4.0 से 4.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी व 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नाली बना लेते हैं| इन नालियों के दोनों किनारे पर 60 से 75 सेंटीमीटर (गर्मी वाली फसल) व 80 से 85 सेंटीमीटर (वर्षाकालीन फसल) की दूरी पर बीज की बुआई करते हैं| एक स्थान पर 2 से 3 बीज 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए| बुवाई के समय बीज का नुकीला भाग नीचे की तरफ रखना चाहिए|
लौकी की खेती के लिए सिंचाई प्रबंधन
घिया (लौकी) की खरीफ ऋतु में खेत की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है| परन्तु वर्षा न होने पर 10 से 15 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है| अधिक वर्षा की स्थिति में जल के निकास के लिए नालियों का गहरा व चौड़ा होना आवश्यक है| गर्मियों में अधिक तापमान होने के कारण 4 से 5 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई करनी चाहिए|
लौकी की फसल में खरपतवार नियंत्रण
घिया (लौकी) की दोनों ऋतु की फसल में सिंचाई के बाद खेत में काफी मात्रा में खरपतवार उग आते हैं| इसलिए उनको किसी कृषि यंत्र की सहायता से 25 से 30 दिनों तक निकाई करके खरपतवार निकालते रहना चाहिए| लौकी में पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 2 से 3 बार निकाई-गुड़ाई करके जड़ों के पास हल्की मिट्टी चढ़ा देना चाहिए| रासायनिक खरपतवारनाशी के रूप में ब्यूटाक्लोर रसायन की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुआई के तुरन्त बाद छिड़काव करना चाहिए|
यह भी पढ़ें- कद्दू वर्गीय सब्जियों में जड़ गांठ सूत्रकृमि की रोकथाम
लौकी की फसल को सहारा देना
वर्षा ऋतु में घिया (लौकी) की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए लकड़ी या लोहे के द्वारा निर्मित मचान पर चढ़ा कर खेती करनी चाहिए| इससे फलों का आकार सीधा एवं रंग अच्छा रहता है और बढ़वार भी तेजी से होती है| प्रारम्भिक अवस्था में निकलने वाली कुछ शाखाओं को काटकर निकाल देना चाहिए, इससे ऊपर विकसित होने वाली शाखाओं में फल ज्यादा बनते हैं| आमतौर पर मचान की ऊँचाई 5.0 से 5.5 फीट तक रखते हैं| इस पद्धति के उपयोग से सस्य क्रिया सम्बन्धित लागत कम हो जाती है|
लौकी की फसल में कीट रोकथाम
कद्दू का लाल कीट (रेड पम्पकिन बिटिल)- इस कीट का वयस्क चमकीली नारंगी रंग का होता हैं और सिर, वक्ष एवं उदर का निचला भाग काला होता है| सूण्ड़ी जमीन के अन्दर पायी जाती है| इसकी सूण्डी व वयस्क दोनों क्षति पहुँचाते हैं| प्रौढ़ पौधों की छोटी पत्तियों पर ज्यादा क्षति पहुँचाते हैं| ग्रब इल्ली मिटटी में रहती है, जो पौधों की जड़ पर आक्रमण कर हानि पहुँचाती है|
ये कीट जनवरी से मार्च के महीनों में सबसे अधिक सक्रिय होते है| अक्टूबर तक खेत में इनका प्रकोप ज्यादा रहता है| नये और छोटे पौधे आक्रमण के कारण मर जाते हैं| फसलों के बीजपत्र एवं 4 से 5 पत्ती अवस्था इन कीटों के आक्रमण के लिए सबसे अनुकूल है| प्रौढ़ कीट विशेषकर मुलायम पत्तियाँ अधिक पसन्द करते है| अधिक आक्रमण होने से पौधे पत्ती रहित हो जाते है|
रोकथाम- सुबह ओस पड़ने के समय राख का बुरकाव करने से भी प्रौढ़ पौधा पर नहीं बैठता जिससे नुकसान कम होता है| जैविक विधि से नियंत्रण के लिए अजादीरैक्टिन 300 पी पी एम 5 से 10 मिलीलीटर प्रति लीटर या अजादीरैक्टिन 5 प्रतिशत 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से दो या तीन छिड़काव करने से लाभ होता है| इस कीट का अधिक प्रकोप होने पर कीटनाशी जैसे डाईक्लोरोवास 76 ई सी 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर या ट्राइक्लोफेरान 50 ई सी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस एल 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से 10 दिनों के अन्तराल पर पर्णीय छिड़काव करें|
यह भी पढ़ें- खीरा की खेती: किस्में, प्रबंधन, देखभाल और पैदावार
फल मक्खी– इस कीट की सूण्डी अधिक हानिकारक होती है| प्रौढ़ मक्खी गहरे भूरे रंग की होती है, इसके सिर पर काले और सफेद धब्बे पाये जाते हैं| प्रौढ़ मादा छोटे, मुलायम फलों के छिलके के अन्दर अण्डा देना पसन्द करती है, और अण्डे से सूड़ी (ग्रब्स) निकलकर फलों के अन्दर का भाग खाकर नष्ट कर देते हैं| कीट फल के जिस भाग पर अण्डा देती है, वह भाग वहाँ से टेढ़ा होकर सड़ जाता है तथा नीचे गिर जाता है|
रोकथाम- गर्मी की गहरी जुताई या पौधे के आस पास खुदाई करें, ताकि मिट्टी की निचली परत खुल जाए जिससे फल मक्खी का प्यूपा धूप द्वारा नष्ट हो जाये या शिकारी पक्षियों के खाने से नष्ट हो, जो भी ग्रसित फल हो इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए| नर फल मक्खी को नष्ट करने के लिए प्लास्टिक की बोतलों में इथेनाल, कीटनाशक (डाईक्लोरोवास या कार्बारिल या मैलाथियान), क्यूल्यूर को 6:1:2 के अनुपात के घोल में लकड़ी के टूकड़े को डुबोकर, 25 से 30 फंदा खेत में विभिन्न स्थानों पर स्थापित कर देना चाहिए|
कार्बारिल 50 डब्ल्यू पी 2 ग्राम प्रति लीटर या मैलाथियान 50 ई सी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी को लेकर 10 प्रतिशत शीरा या गुड़ में मिलाकर जहरीले चारे को 250 जगहों पर प्रति हेक्टेयर खेत में उपयोग करना चाहिए| प्रतिकर्षी 4 प्रतिशत नीम की खली का प्रयोग करें, जिससे जहरीले चारे की ट्रैपिंग की क्षमता बढ़ जाये| आवश्यकतानुसार कीटनाशी जैसे क्लोरेंट्रानीलीप्रोल 18.5 एस सी 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर या डाईक्लारोवास 76 ई सी 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से भी छिड़काव कर सकते हैं|
लौकी की फसल में रोग रोकथाम
चूर्णील आसिता- रोग का प्रथम लक्षण पत्तियों तथा तनों की सतह पर सफेद या धुंधले धूसर रंग के पावडर जैसा दिखाई देता है| कुछ दिनों के बाद वे धब्बे चूर्णयुक्त हो जाते हैं| सफेद चूर्णी पदार्थ अंत में समूचे पौधे की सतह को ढंक लेता है| अधिक प्रकोप के कारण फलों का आकार छोटा रह जाता है|
रोकथाम- रोकथाम के लिए रोग पीड़ित पौधों के खेत में फफूंदनाशक दवा जैसे 0.05 प्रतिशत ट्राइडीमोर्फ 1 से 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोलकर सात दिन के अंतराल पर छिड़काव करें| इस दवा के उपलब्ध न होने पर फ्लूसिलाजोल 1 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर या माईक्लोबूटानिल 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के साथ 7 से 10 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें|
यह भी पढ़ें- करेला की खेती: किस्में, प्रबंधन, देखभाल और पैदावार
मृदुरोमिल फफूदी- यह रोग वर्षा और ग्रीष्म कालीन दोनों फसल में समान रूप से आता है| उत्तरी भारत में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है| इस रोग के मुख्य लक्षण पत्तियों पर कोणीय धब्बे जो शिराओं द्वारा सीमित होते हैं| ये कवक पत्ती के ऊपरी पृष्ठ पर पीले रंग के होते हैं और नीचे की तरफ रोयेंदार वृद्धि करते हैं|
रोकथाम- बचाव के लिए बीजों को मेटलएक्सिल नामक कवकनाशी की 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए और मैंकोजेब 0.25 प्रतिशत घोल का छिड़काव रोग के लक्षण प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद फसल पर करना चाहिए| यदि संक्रमण उग्र दशा में हो तो मैटालैक्सिल + मैंकोजेब का 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से या डाइमेयामर्फ का 1 ग्राम प्रति लीटर + मैटीरैम का 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से 7 से 10 के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव करें|
मोजैक विषाणु रोग- यह रोग विशेषकर नई पत्तियों में चितकबरापन तथा सिकुड़न के रूप में प्रकट होता है| पत्तियाँ छोटी तथा हरी पीली हो जाती है| संक्रमित पौधे की वृद्धि रूक जाती है| इसके आक्रमण से पर्ण छोटे तथा पुष्प छोटे-छोटे पत्तियों जैसे बदले हुए दिखाई पड़ते हैं| ग्रसित पौधा बौना रह जाता है, और उसमें फलत बिल्कुल नहीं होता है|
रोकथाम- बचाव के लिए रोग ग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए| रोग वाहक कीटों से बचाव के करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.3 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर दस दिनों के अन्तराल में 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करना चाहिए| कीट और रोग रोकथाम की अधिक जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें- कद्दू वर्गीय सब्जियों के कीट एवं रोग और उनका नियंत्रण कैसे करें
लौकी फसल के फलों की तुड़ाई
घिया (लौकी) के फलों की तुड़ाई मुलायम अवस्था में करनी चाहिए| फलों का वजन किस्मों पर निर्भर करता है| फलों की तुड़ाई डण्ठल लगी अवस्था में किसी तेज चाकू से चार से पाँच दिन के अंतराल पर करना चाहिए, ताकि पौधे पर ज्यादा फल लगे|
लौकी की खेती से पैदावार
उपरोक्त वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने पर औसतन घिया (लौकी) की पैदावार 35 से 60 टन प्रति हेक्टेयर होती हैं|
यह भी पढ़ें- खरबूजे की खेती: जाने किस्में, देखभाल और पैदावार
अगर आपको यह लेख पसंद आया है, तो कृपया वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें| आप हमारे साथ Twitter और Facebook के द्वारा भी जुड़ सकते हैं|
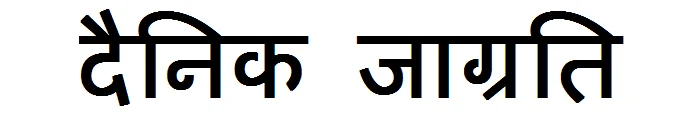
Leave a Reply