
एक कलेक्टर जिले में एक सरकारी प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसकी भूमिका जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की होती है| एक जिला कलेक्टर जिले में पुलिस और अभियोजन विभाग का प्रमुख होता है| जिला कलेक्टर को भारत में कई राज्यों में उपायुक्त के रूप में भी जाना जाता है| यह भारत में सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों में से एक है|
कई छात्रों का कलेक्टर बनने का सपना होता है| क्या आप उनमें से एक हैं? यदि हाँ, और जानना चाहते हैं कि जिला कलेक्टर कौन होते हैं और कलेक्टर कैसे बनते हैं तो यह लेख आपके लिए है| इस लेख में, हम जिला कलेक्टर कैसे बनें, इसकी पूरी जानकारी पर चर्चा करेंगे|
यूपीएससी हर साल उन लाखों उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि अधिकारी बनना चाहते हैं| इसलिए, कलेक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा देनी होगी| उम्मीदवार जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में उत्तीर्ण हैं, वे यूपीएससी सिविल सेवा फॉर्म के लिए आवेदन करने के पात्र हैं|
यह भी पढ़ें- एनआईए क्या है? एनआईए ऑफिसर कैसे बने
कलेक्टर कौन है?
कलेक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्य में एक उच्च अधिकारी होता है और उसका काम किसी विशेष जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना और एक जिले में भू-राजस्व एकत्र करना होता है| एक कलेक्टर एक जिले में पुलिस विभाग और अभियोजन एजेंसी का प्रमुख होता है| एक कलेक्टर के पास भारत के कानून को तोड़े बिना उस जिले के विकास के लिए कुछ भी करने की शक्ति है| मूल रूप से, एक कलेक्टर एक जिले में प्रशासन का प्रमुख होता है| एक कलेक्टर को भारत की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है|
कलेक्टर वह व्यक्ति होता है जो उस जिले के विकास के लिए सभी योजनाओं को पारित करता है| एक कलेक्टर के पास किसी भी अधिकारी को निलंबित करने की शक्ति होती है जो उचित तरीके से अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है| अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी हिंसा को बेअसर करना कलेक्टर की जिम्मेदारी है| इसलिए, एक कलेक्टर वह व्यक्ति होता है जो जिले में विभिन्न कार्यों को संभालता है|
इसके लिए परीक्षा दो प्रकार की होती है एक यूपीएससी की परीक्षा और दूसरी एसपीएससी की परीक्षा जिसमें से आप कोई एक परीक्षा देकर कलेक्टर बन सकते हैं| सिविल सेवा परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) द्वारा आयोजित की जाती है|
यह भी पढ़ें- सीबीआई ऑफिसर कैसे बने: योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, करियर
कलेक्टर बनने के लिए पात्रता मानदंड
जो अभ्यर्थी कलेक्टर बनना चाहते हैं, उनके पास परीक्षा में बैठने से पहले ये योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे-
शैक्षणिक योग्यता
उम्मीदवारों के पास कलेक्टर बनने के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जैसे-
1. उम्मीदवारों को शिक्षा के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए|
2. कलेक्टर बनने के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए|
3. किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवार फॉर्म के लिए आवेदन करने के पात्र हैं|
4. जो उम्मीदवार स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी प्रीलिम्स फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं|
5. तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों डिग्री-आधारित छात्र परीक्षा के लिए पात्र हैं|
आयु सीमा
यूपीएससी या एसपीएससी फॉर्म के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए| अधिकतम आयु सीमा श्रेणी दर श्रेणी पर निर्भर करती है| हालांकि, आरक्षण के कारण कुछ श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में छूट मिलती है, जैसे-
सामान्य श्रेणी: कलेक्टर बनने के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा दिए जा सकने वाले प्रयासों की अधिकतम संख्या 6 है|
ओबीसी श्रेणी: कलेक्टर बनने के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है और ओबीसी (अन्य पिछड़ी जाति) श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा दिए जा सकने वाले प्रयासों की अधिकतम संख्या 9 है|
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी: कलेक्टर बनने के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा दिए जा सकने वाले प्रयासों की अधिकतम संख्या अनंत है|
शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार: कलेक्टर बनने के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है और शारीरिक रूप से अक्षम या पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा दिए जा सकने वाले प्रयासों की अधिकतम संख्या 9 (सामान्य और ओबीसी श्रेणी के लिए) और असीमित (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आयु सीमा तक)|
राष्ट्रीयता
1. भारत का नागरिक भारत में कलेक्टर बनने के योग्य है|
2. नेपाल, भूटान और तिब्बत जैसे देशों के नागरिक भारत में कलेक्टर बनने के पात्र हैं|
यह भी पढ़ें- डॉक्टर कैसे बने: पात्रता, कौशल, कर्तव्य, करियर और वेतन
कलेक्टर की भूमिका और उत्तरदायित्व
जिला कलेक्टर की भूमिका और उत्तरदायित्व इस प्रकार है, जैसे-
1. एक जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी एक कलेक्टर की होती है|
2. एक जिले में भू-राजस्व के संग्रह के लिए एक कलेक्टर की जिम्मेदारियां होती हैं|
3. एक कलेक्टर वह व्यक्ति होता है जो आयकर बकाया, सिंचाई बकाया, उत्पाद शुल्क आदि के संग्रह के लिए जिम्मेदार होता है|
4. एक कलेक्टर अपने जिले में भूमि अभिलेखों के रखरखाव और जोत की चकबंदी के लिए जिम्मेदार होता है|
5. एक कलेक्टर वह व्यक्ति होता है जो लोगों को सभी कृषि ऋण देता है|
6. एक कलेक्टर जिला औद्योगिक केंद्र का प्रमुख होता है|
7. एक कलेक्टर जिला कार्यकारी मजिस्ट्रेट का प्रमुख होता है|
8. कलेक्टर वह व्यक्ति होता है जो अपने जिले में किसी प्राकृतिक आपदा में आपदा प्रबंधन का प्रमुख बनता है|
9. एक कलेक्टर एक जिले का मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) होता है|
10. वह सभी सरकारी योजनाओं को पारित करता है जो जिले के विकास के लिए है|
यह भी पढ़ें- UPSC Exam क्या है-पात्रता, योग्यता और चयन प्रक्रिया
कलेक्टर बनने के लिए परीक्षा
इस के लिए दो तरह के एग्जाम होते हैं जिनसे आप कलेक्टर बन सकते हैं, जैसे-
1. यूपीएससी परीक्षा
2. एसपीएससी परीक्षा
यूपीएससी परीक्षा: सिविल सेवा परीक्षा भारत के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है| यह एक अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा है जो हर साल आयोजित की जाती है| परीक्षा का तरीका पेन-पेपर मोड (ऑफ़लाइन) है| यूपीएससी भारत की केंद्र सरकार के अधीन आता है और अगर यूपीएससी में कोई बदलाव किया जाना है तो यह केंद्र सरकार के हाथ में है|
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अगर कोई बदलाव करना होता है तो यूपीएससी ही करता है| यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है| आमतौर पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा फॉर्म फरवरी से मार्च के महीने में आता है और जो परीक्षा होती है वह अक्टूबर के महीने में होती है| यूपीएससी परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है, जैसे-
I. प्रारंभिक परीक्षा
प्रारंभिक परीक्षा को यूपीएससी प्रीलिम्स के नाम से भी जाना जाता है| यूपीएससी प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला चरण है| प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं – एक सामान्य अध्ययन पेपर- I के लिए होता है और दूसरा सामान्य अध्ययन पेपर- II के लिए होता है| पेपर- I में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक वाले 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाते हैं|
पेपर II में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.5 अंक वाले 80 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाते हैं| प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे है और प्रश्न प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) है| प्रारंभिक परीक्षा में कुल 400 अंक होते हैं|
सामान्य अध्ययन पेपर- I का पाठ्यक्रम
1. भारतीय और विश्व भूगोल
2. आर्थिक और सामाजिक विकास
3. भारत का इतिहास
4. अंतरराष्ट्रीय राजनीति
5. राष्ट्रीय की वर्तमान घटनाएँ
6. विश्व इतिहास
7. भारतीय राजनीति और शासन
8. अंतर्राष्ट्रीय संबंध महत्व
9. सामान्य विज्ञान
10. जैव-विविधता और जलवायु परिवर्तन
11. पर्यावरण पारिस्थितिकी पर सामान्य मुद्दा, इत्यादि|
यह भी पढ़ें- सेना की नौकरी कैसे प्राप्त करें: योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, कौशल
सामान्य अध्ययन पेपर- II का पाठ्यक्रम
1. तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता
2. सामान्य मानसिक क्षमता
3. समझ
4. निर्णय लेना और समस्या समाधान
5. संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल
6. आंकड़ा निर्वचन
7. मूल अंकज्ञान, इत्यादि|
II. मुख्य परीक्षा
मुख्य परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा का दूसरा चरण है| आप प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद मुख्य परीक्षा देने के योग्य होते हैं| मुख्य परीक्षा में कुल 1750 अंक होते हैं| यूपीएससी मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं| प्रत्येक पेपर का विवरण इस प्रकार है, जैसे-
निबंध लेखन (पेपर 1)
यह एक निबंध लेखन पेपर है जिसमें कुल 250 अंक होते हैं| इस पेपर में आपको 3 घंटे की अवधि मिलेगी और 3 घंटे की अवधि के भीतर आपको 1000 से 1200 औसत शब्दों के किसी भी विषय पर 2 उचित निबंध लिखने होंगे|
सामान्य अध्ययन I (पेपर 2)
यह एक सामान्य अध्ययन आधारित पेपर है जिसमें कुल 250 अंक हैं और इसकी कुल अवधि 3 घंटे है| सामान्य अध्ययन I में भारतीय समाज, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव, विश्व भौतिक भूगोल, भौगोलिक विशेषताएं, विश्व इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, पूंजीवाद आदि जैसे विषय शामिल हैं|
सामान्य अध्ययन II (पेपर 3)
यह सामान्य अध्ययन II भारतीय संविधान, संसद, राज्य विधानसभाओं, न्यायपालिका मंत्रालयों, सरकार के विभागों, विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकायों, विवाद निवारण तंत्र, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, कल्याण योजनाओं, कानून, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दों, नीतियों का प्रभाव, और बहुत कुछ जैसे विषयों को शामिल करता है| पेपर की अवधि 3 घंटे है और इसमें कुल 250 अंक हैं|
सामान्य अध्ययन III (पेपर 4)
इसमें उपरोक्त पेपर के समान अंक होते हैं और पेपर की अवधि भी उपरोक्त के समान ही होती है| इसके कवर के कुछ विषय सरकारी बजट, भारत में भूमि सुधार, अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था, खाद्य प्रसंस्करण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचा आदि हैं|
यह भी पढ़ें- कोर्ट क्लर्क कैसे बने: पात्रता, आवेदन, कर्तव्य, वेतन
सामान्य अध्ययन IV (पेपर 5)
सामान्य अध्ययन IV के अंतर्गत आने वाला पाठ्यक्रम नैतिकता, दृष्टिकोण, अखंडता, निष्पक्षता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता अवधारणाएँ, परिवार की भूमिका, लोक प्रशासन में नैतिकता, शासन में सत्यनिष्ठा, सेवा वितरण की गुणवत्ता आदि है| इसमें कुल 250 अंक होते हैं और अवधि 3 घंटे है|
वैकल्पिक विषय I (पेपर 6)
आपको यूपीएससी में वैकल्पिक विषयों की सूची में से किसी एक विषय को चुनना होगा| इस वैकल्पिक विषय की अवधि 3 घंटे है और इसमें कुल 250 अंक हैं|
वैकल्पिक विषय II (पेपर 7)
मानदंड उपरोक्त वैकल्पिक विषय के पेपर के समान हैं|
भारतीय भाषा का पेपर (पेपर 8)
यह यूपीएससी मुख्य परीक्षा में अनिवार्य आधारित भाषा का पेपर है| इसमें कुल 300 अंक होते हैं और इस पेपर की अवधि 3 घंटे होती है|
अंग्रेजी भाषा का पेपर (पेपर 9)
यह केवल एक अंग्रेजी आधारित भाषा का पेपर है| कुल अंक और अवधि उपरोक्त भाषा-आधारित पेपर के समान हैं|
वैकल्पिक विषय
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में वैकल्पिक विषय इस प्रकार हैं, जैसे-
कृषि, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, असैनिक अभियंत्रण, वाणिज्य और लेखा, अर्थशास्त्र, विद्युत अभियन्त्रण, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, इतिहास, कानून, प्रबंध, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, समाज शास्त्र, आंकड़े और प्राणि विज्ञान आदि|
III. साक्षात्कार परीक्षण
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अगला और अंतिम चरण साक्षात्कार होता है| आपको पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट देना होगा| साक्षात्कार प्रक्रिया में 275 अंक होते हैं| साक्षात्कार प्रक्रिया में आपके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाते हैं| इंटरव्यू प्रक्रिया में आपसे तरह-तरह के सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको मौखिक रूप से देना होगा और इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान आपका व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि आपको व्यक्तित्व में भी अंक मिलेंगे|
साक्षात्कार चरण में अर्हता प्राप्त करने के बाद आपको पहले प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और प्रशिक्षण अवधि पूरी करने के बाद आप किसी भी जिले में पदस्थापित होने के लिए तैयार होते हैं|
नोट:- प्रारंभ में आपका कलेक्टर के पद पर पदस्थापन नहीं हो सकता है|
एसपीएससी परीक्षा: एसपीएससी भी एक सिविल सेवा परीक्षा है लेकिन यह राज्य सरकार के अधीन आती है| भारत में हर राज्य अपनी एसपीएससी परीक्षा आयोजित करता है| एसपीएससी (SPSC) राज्य लोक सेवा आयोग के लिए खड़ा है और यह राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित किया जाता है| एसपीएससी परीक्षा का पाठ्यक्रम यूपीएससी परीक्षा के समान ही है| इस परीक्षा के माध्यम से आप कलेक्टर बन सकते हैं लेकिन कलेक्टर बनने में कई साल और पदोन्नति लगती है क्योंकि शुरुआत में कलेक्टर की तुलना में आपको निम्न ग्रेड पद प्राप्त होंगे| एसपीएससी परीक्षा भी तीन चरणों में आयोजित की जाती है, जैसे-
1. प्रारंभिक
2. मुख्य
3. साक्षात्कार|
यह भी पढ़ें- डाक सहायक भर्ती: योग्यता, चयन प्रक्रिया, कौशल, वेतन
भारत में कलेक्टर का वेतन
भारत में कलेक्टरों के वेतन की औसत सीमा एक महीने में 56,000 रुपये से 1,50,000 रुपये है| हालांकि, वेतन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि सेवा में आवश्यक वर्षों की संख्या, अनुभव, प्रदर्शन, स्थान आदि| कलेक्टर को चिकित्सा, यात्रा, आवास, पेंशन, सुरक्षा, अवकाश जैसे कई प्रकार के भत्ता लाभ भी दिए जाते हैं|
कलेक्टर के लिए सुविधाएं
1. एक कलेक्टर को एक निजी परिवहन वाहन मिलता है|
2. एक कलेक्टर को हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है|
3. एक कलेक्टर को व्यक्तिगत सुरक्षा मिलती है|
4. एक कलेक्टर को उसके आवंटित जिले में एक निजी सरकारी बंगला मिलता है|
5. एक कलेक्टर को 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश मिलता है|
6. एक कलेक्टर कार्यालय के काम के लिए जहां भी जाते हैं उन्हें परिवहन की सुविधा मिल जाती है|
7. एक कलेक्टर को महंगाई भत्ता मिलता है|
8. एक कलेक्टर को सरकार से यात्रा और अवकाश की सुविधा मिलती है|
यह भी पढ़ें- डाक सेवा में करियर: पात्रता, भर्ती प्रक्रिया, वेतन और कैरियर
कलेक्टर बनने के लिए कदम
चरण 1: सिविल सेवा परीक्षा फॉर्म को लागू करें|
चरण 2: प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित हों और इसके लिए अर्हता प्राप्त करें|
चरण 3: उसके बाद, मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित हों और इसके लिए अर्हता प्राप्त करें|
चरण 4: उसके बाद साक्षात्कार में उपस्थित हों और एक उचित साक्षात्कार दें|
स्टेप 5: इंटरव्यू प्रक्रिया में क्वालीफाई करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा|
चरण 6: प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात आप किसी भी जिले में कलेक्टर के पद पर पदस्थापित होने के लिए तैयार हैं|
यह भी पढ़ें- डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने: करियर, कार्यक्षेत्र, नौकरियां, वेतन
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: कलेक्टर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए?
उत्तर: उम्मीदवारों को किसी भी विषय से स्नातक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है|
प्रश्न: कौन सी परीक्षा देकर हम कलेक्टर बन सकते हैं?
उत्तर: आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या एसपीएससी परीक्षा देकर कलेक्टर बन सकते हैं|
प्रश्न: क्या मैं 12वीं के बाद कलेक्टर बन सकता हूँ?
उत्तर: नहीं, कलेक्टर बनने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है|
प्रश्न: भारत में कलेक्टर का वेतन क्या है?
उत्तर: भारत में एक कलेक्टर का औसत वेतन 56,000 रुपये से 1,50,000 रुपये प्रति माह है|
प्रश्न: क्या कोई खिलाड़ी कलेक्टर बन सकता है?
उत्तर: हां, एक खेल खिलाड़ी कलेक्टर बनता है लेकिन एक खेल खिलाड़ी के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और एक खेल खिलाड़ी को सिविल सेवा परीक्षा के सभी स्तरों के लिए अर्हता प्राप्त करनी होती है|
प्रश्न: जिला कलेक्टर बनने की अधिकतम आयु क्या है?
उत्तर: सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष है| ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष है और एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है|
प्रश्न: क्या कोई लड़की जिला कलेक्टर बन सकती है?
उत्तर: जी हां, एक लड़की जिलाधिकारी बन सकती है|
प्रश्न: क्या कलेक्टर बनना कठिन है?
उत्तर: कलेक्टर परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है और आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी जल्दी शुरू करनी होगी| 5वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन शुरू करें| यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए आपको रोजाना कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करनी होगी|
प्रश्न: कलेक्टर के लिए कौन सी स्ट्रीम सबसे अच्छी है?
उत्तर: कलेक्टर बनने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री पूरी करनी होगी इसके लिए आप अपनी 12वीं कक्षा में कोई भी विषय चुन सकते है| लेकिन मेरा सुझाव है कि आप 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित का चयन करें क्योंकि यह भविष्य में कलेक्टर बनने के आपके लक्ष्य में आपकी मदद करेगा|
प्रश्न: क्या अत्यावश्यकता की स्थिति में जिला कलेक्टर को अवकाश मिल सकता है?
उत्तर: हाँ, जिला कलक्टरों को अत्यावश्यकता की स्थिति में अवकाश मिलता है|
यह भी पढ़ें- एलडीसी कैसे बने: पात्रता, कौशल, करियर और भर्ती प्रक्रिया
अगर आपको यह लेख पसंद आया है, तो कृपया वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें| आप हमारे साथ Twitter और Facebook के द्वारा भी जुड़ सकते हैं|
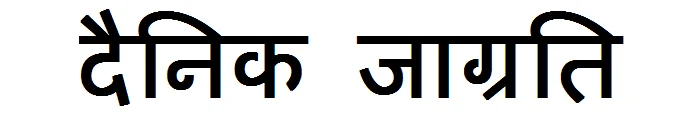
Leave a Reply